विचार: सत्ता के संस्कार बदलने का अनुष्ठान
नाम बदलना ‘स्वत्व’ की वापसी का शंखनाद है, जिसे भावुकता कहकर नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को इस सत्य से भी आंखें मिलानी होंगी कि ‘लकड़हारे की कुल्हाड़ी’ केवल नाम से नहीं, अपनी धार से पहचानी जाती है। यदि ‘कर्तव्य पथ’ या ‘लोक भवन’ में बैठा तंत्र उसी औपनिवेशिक ठसक से ग्रस्त रहा, तो यह बदलाव अधूरा माना जाएगा। अफसर के मन से ‘रूलर’ होने का भ्रम मिटाना ही इस बदलाव की असली कसौटी है। चुनौती अब नाम की नहीं, व्यवस्था के डीएनए में भारतीयता के प्राण फूंकने की है।
HighLights
अफसर को याद दिलाता है कि वह मालिक नहीं, सेवक है
रामानंद शर्मा। रायसीना हिल्स पर इन दिनों जो हो रहा है, वह साधारण नहीं है। वहां सिर्फ इमारतें नहीं बन रहीं, बल्कि एक पुरानी और जंग लगी मानसिकता ढह रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब ‘सेवा-तीर्थ’ होगा और राजभवन ‘लोक भवन’। लुटियंस दिल्ली के कुलीन हलकों में इसे लेकर सवाल है कि क्या यह सिर्फ नेमप्लेट बदलने की रस्म है? जवाब है-नहीं। यह उस औपनिवेशिक आत्मा से मुक्ति का अनुष्ठान है, जो आजादी के बाद भी हम पर हावी रही। शब्द सिर्फ बोलते नहीं, वे सोचते भी हैं। अंग्रेजों ने भारत पर सिर्फ बंदूक से राज नहीं किया, उन्होंने शब्दों से हमें गुलाम बनाया। उन्होंने खुद को ‘शासक’ और हमें ‘प्रजा’ माना। वह ढांचा ‘हुकूमत’ के लिए था, ‘सेवा’ के लिए नहीं।
जब पीएमओ ‘सेवा-तीर्थ’ बनता है, तो वह सत्ता के गलियारों में बैठे अफसर को याद दिलाता है कि वह मालिक नहीं, सेवक है। यह बदलाव ईंट-गारे का नहीं, उस ‘लौह-ढांचे’ को पिघलाने का है, जिसे हमने 75 साल तक ओढ़े रखा। यह भाषाई गुलामी के पिंजरे को तोड़ने की एक जरूरी और साहसिक शुरुआत है। इसे राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की नजर से देखिए। ‘कलेक्टर’ शब्द को देखिए। आखिर जिले के मुखिया को कलेक्टर क्यों कहा जाता है? इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो जवाब वर्ष 1772 में मिलेगा। यह वारेन हेस्टिंग्स की ईजाद थी। उस वक्त मकसद ‘जनसेवा’ नहीं, सिर्फ लगान ‘कलेक्ट’ करना था। ‘कलेक्टर’ शब्द में ‘लेने’ का भाव है, ‘देने’ का नहीं। यह शब्द कुर्सी पर बैठने वाले के दिमाग में ‘माई-बाप’ होने का अहंकार भर देता है, जबकि हमारा संविधान ‘कल्याणकारी राज्य’ की बात करता है। कौटिल्य ने यूं ही प्रशासनिक प्रमुख के लिए ‘समाहर्ता’ शब्द नहीं चुना था। समाहर्ता यानी वह, जो बिखरे हुए को सहेजे, जो समाज के सूत्रों को जोड़े। अंग्रेज ‘कलेक्टर’ महज उगाही जानता था। इसके विपरीत भारतीय चिंतन के ‘समाहर्ता’ का मर्म ‘पोषण’ में है, प्रजा के योगक्षेम में है।
प्रधानमंत्री कार्यालय को ‘सेवा-तीर्थ’ कहना सत्ता का चरित्र-बदल की कोशिश है। ‘सेवा-तीर्थ’ सामंती मानसिकता पर चोट है। जब दफ्तर ‘तीर्थ’ बन जाता है, तो वहां झूठ बोलना या रिश्वत लेना अपराध नहीं ‘पाप’ हो जाता है। यह नैतिक दबाव है। यह सत्ता को ‘भोग’ से खींचकर ‘सेवा’-‘साधना’ के धरातल पर लाता है। आलोचक इसे रंग दे सकते हैं, पर यह उस भारतीयता की वापसी है जहां सेवा परम धर्म है।
राजभवन को ‘लोक भवन’ कहना भी लोकतंत्र के आत्मा की वापसी जैसा है। संविधान की शुरुआत ‘हम भारत के लोग’ से होती है, ‘हम भारत के राजा’ से नहीं। जब बुनियाद ‘लोक’ है, तो इमारत ‘राज’ वाली क्यों? सामंती बोर्ड क्यों टंगे रहें? ‘राजभवन’ शब्द उस ‘लाट-साहबी’ दौर की याद है, जब शासक ऊंची हवेलियों में जनता से दूर रहता था। ‘राज’ शब्द शासक और शासित के बीच की खाई को गहरा करता है।
सरकार की नीयत साफ है और दिशा भी, लेकिन अभी जो हो रहा है, वह ‘तदर्थवाद’ है। कहीं कोई शहर का नाम बदल रहा है, कहीं कोई सड़क का। इसमें न कोई एकरूपता है, न वैज्ञानिक दृष्टि। इससे विवाद उपजते हैं। वक्त आ गया है कि इस प्रक्रिया को संस्थागत जामा पहनाया जाए। सरकार को एक वैधानिक ‘राष्ट्रीय नामकरण एवं प्रशासनिक शब्दावली सुधार आयोग’ का गठन करना चाहिए। नाम बदलना एक गंभीर सांस्कृतिक विमर्श होना चाहिए। इस आयोग में नेताओं की जगह इतिहासकार, भाषाविद और समाजशास्त्री बैठें। नाम बदलने की प्रक्रिया को ‘राजनीतिक लाभ’ के चश्मे से हटाकर ‘सांस्कृतिक पुनर्जागरण’ के रूप में स्थापित करना होगा।
भारत की एकता उसकी विविधता में है। अगर तमिलनाडु में बदलाव हो तो वहां ‘कोट्टम’ या ‘नाडु’ जैसे शब्द गूंजें। महाराष्ट्र में शिवाजी के ‘अष्टप्रधान’ की धमक हो। इससे न केवल गुलामी के निशान मिटेंगे, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं का स्वाभिमान भी लौटेगा। जिन्हें यह बदलाव ‘संकीर्ण राष्ट्रवाद’ लगता है, वे जरा दुनिया देखें। भारत अकेला नहीं है। यह एक वैश्विक शुद्धि यज्ञ है, जिसे दुनिया ‘डीकोलोनाइजेशन’ कहती है। दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद मिटने के बाद ‘पोर्ट एलिजाबेथ’ (अब गकेबरहा) जैसे कई शहरों के नाम बदले, ताकि वहां के मूल निवासियों को उनकी खोई हुई पहचान वापस मिल सके। न्यूजीलैंड अपनी माओरी संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहा है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। वहां उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत ‘माउंट मैकिंले’ का नाम बदलकर, मूल निवासियों की पहचान ‘डिनाली’ कर दिया गया। नाम बदलना यह बताने का प्रयास है कि हमारे नायक ‘क्लाइव’ और ‘डलहौजी’ नहीं, बल्कि ‘चाणक्य’, ‘तिरुवल्लुवर’ और ‘गांधी’ हैं।
नाम बदलना ‘स्वत्व’ की वापसी का शंखनाद है, जिसे भावुकता कहकर नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को इस सत्य से भी आंखें मिलानी होंगी कि ‘लकड़हारे की कुल्हाड़ी’ केवल नाम से नहीं, अपनी धार से पहचानी जाती है। यदि ‘कर्तव्य पथ’ या ‘लोक भवन’ में बैठा तंत्र उसी औपनिवेशिक ठसक से ग्रस्त रहा, तो यह बदलाव अधूरा माना जाएगा। अफसर के मन से ‘रूलर’ होने का भ्रम मिटाना ही इस बदलाव की असली कसौटी है। चुनौती अब नाम की नहीं, व्यवस्था के डीएनए में भारतीयता के प्राण फूंकने की है।
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)








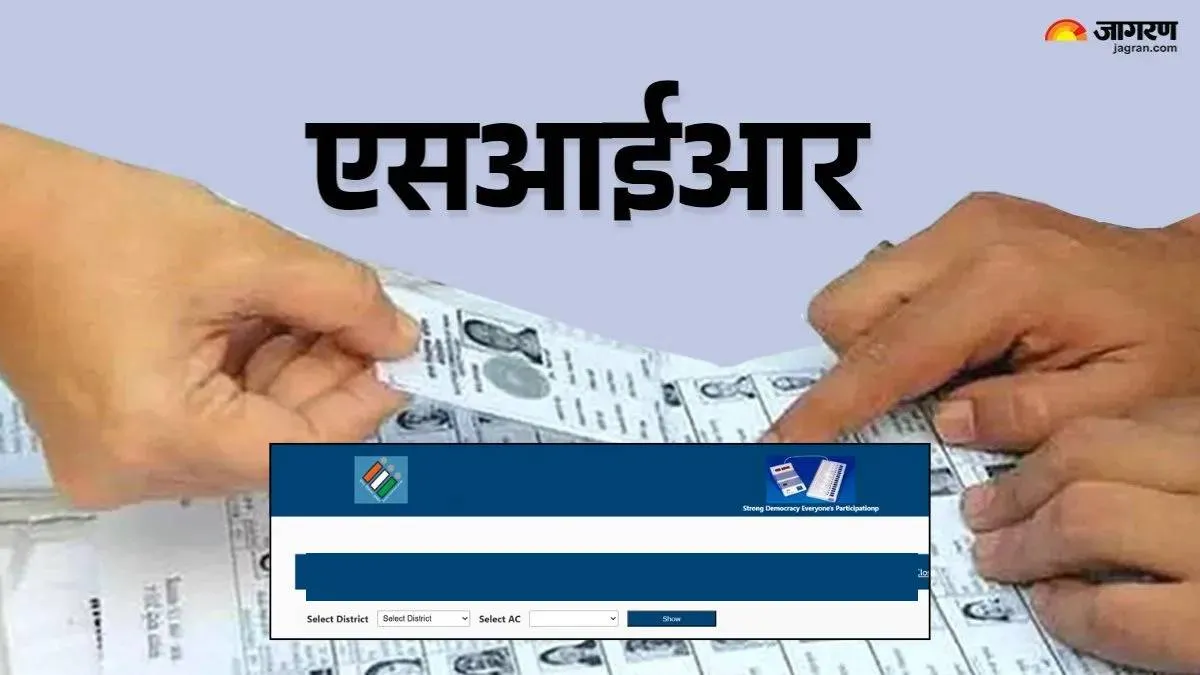




कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।